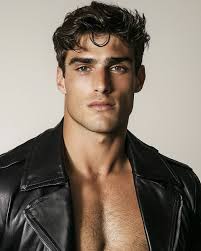कोरोना का होगा अंत और देश बनेगा सेहतमंद.
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

पिछले डेढ़ साल से डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी दुनिया के खुदा है। कोरोना की मार के वक्त अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मियों और डॉक्टरों ने हमारी जिंदगियां बचाई हैं। इस महामारी ने हमें सीखा दिया है कि जान है, तो जहान है। इसलिए नीति-निर्माता इस दिन-रात इस कोशिश में लगे हैं कि कैसे देश का हेल्थ सेक्टर चमचमा जाए। पिछले 75 साल की ओर मुड़कर देखें तो हम पाते हैं कि हमने बीमारियों के खिलाफ अपनी लड़ाई को अधिक मजबूत किया है। इसी का परिणाम है कि भारत में जीवन प्रत्याशा में काफी बढ़ोतरी हुई है, यानी उम्र लंबी हुई है।
विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 1970-75 के दौरान भारत में जीवन प्रत्याशा जहां करीब 51 वर्ष थी, वहीं 2015-19 में यह बढ़कर 69 वर्ष तक पहुंच गई। यही नहीं छह दशकों में बाल मृत्यु दर 81 फीसद कम हो गई है। प्लेग, चेचक, पोलियो, टाइफाइड जैसी बीमारियों पर भी हमने जीत हासिल की है। कोरोना के दौर में हम उन चंद मुल्कों में से एक थे जिन्होंने वैक्सीन का निर्माण किया। यानी अतीत उपलब्धियों की अशर्फियों से भरा रहा है। अब हेल्थ सेक्टर के चार दिग्गजों इंटरनेशनल पीडियाट्रिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर नवीन ठक्कर, पब्लिक हेल्थ फिजिशियन डॉ राजशंकर घोष, पद्मश्री डॉ एम वली और ICMR के वरिष्ठ वैज्ञानिक अमित के डिंडा से जानते हैं कि अगले पांच साल कैसे होने वाले हैं।
इंटरनेशनल पीडियाट्रिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर नवीन ठक्कर कहते हैं कि हेल्थ में काफी तरक्की की है। कोरोना ने एहसास कराया कि भारत जैसी अधिक जनसंख्या वाले देश में बहुत कुछ करना बाकी है। हमें एम्स जैसे मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खोलने की जरूरत है। साथ ही हमें महिलाओं, बच्चों, आदिवासी और दूर दराज में रहने वाले लोगों के लिए कंप्रिहेंसिव प्राइमरी केयर मुहैया करानी होगी।
पब्लिक हेल्थ में ज्यादा निवेश करना होगा। ताकि हम भविष्य में आने वाली महामारी का मुकाबला कर सकें। इंडिया न्यू बार्न एक्शन प्लान नवजात शिशु की मृत्यु दर को कम करना होगा और टीकाकरण के एजेंडे 2030 पर काम करना होगा। क्योंकि भारत में कोई टीका न लगवाने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं कोरोना से सबक लेते हुए हमें हर उम्र के लोगों के लिए बेहतर टीकाकरण सुविधाएं मुहैया करानी होगा।
पब्लिक हेल्थ फिजिशियन डॉ राजशंकर घोष की भी टीकाकरण पर यही राय है। वह कहते हैं कि पिछले 75 साल में देश के स्वास्थकर्मियों ने देश की जनता के साथ मिलकर स्माल पॉक्स और पोलियो जैसी बीमारियां दूर कर चुके हैं। रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी तेजी से बढ़ रहा है। इसमें बच्चों को निमोनिया, मीजल्स, डायरिया जैसी बीमारियों से मुक्ति मिलने के लिए टीका मिलता है। लेकिन अभी ये 30 फीसद बच्चों को यह सुविधा नहीं मिल रहा है। हमें इस दिशा में का करना होगा।
ICMR के वरिष्ठ वैज्ञानिक और एम्स के चीफ कोऑर्डिनेटर सेंटर फॉर मेडिकल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोफेसर अमित के मुताबिक आजादी के समय देश में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की संख्या 725 थी। अब इनकी संख्या 30 हजार के ऊपर पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार ने जो आयुष्मान भारत योजना और जन आरोग्य योजना शुरू की इससे देश के लोगों को बड़ा फायदा हुआ।
सरकार ने नई दवाओं और हेल्थ टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होने के लिए बायो फार्मा मिशन की शुरुआत की है। जल्द ही देश स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होगा। वो दिन दूर नहीं जब भारत पूरी दुनिया में अपनी स्वास्थ्य सेवाओं और तकनीक के लिए जाना जाएगा। वहीं डॉक्टर एम वली कहते हैं कि हेल्थ सेक्टर में हमने विकास किया है लेकिन गांवों तक पर्याप्त सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। इसलिए हमें गांव तक बिजली-पानी-स्कूल जैसी सुविधाएं पहुंचानी होगी ताकि डॉक्टर वहां आसानी से रह सकें और गांव में भी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो सकें।
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि नीति आयोग नेशनल हेल्थ स्टेक नाम की योजना पर काम कर रहा है। इसमें मशीन लर्निंग के साथ बिग डेटा और एआई जैसे एनालिटिक्स प्लेटफार्म का बेहतर तरीके से लाभ उठाते हुए देश की पूरी आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा का बेहतर प्रबंधन किया जाएगा। रिपोर्टों के अनुसार, नागरिकों को विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान पत्र (आईडी) प्रदान किए जाएंगे ताकि माउस के क्लिक पर किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य इतिहास तक पहुंचा जा सके। इससे रोगियों, डॉक्टरों और नीति निर्माताओं की मदद कर सके। इसके अलावा 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है। डायबिटीज की रोकथाम के लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से अभियान चला रही है।
हेल्थ सेक्टर में अगले पांच साल में होंगे ये 5 बदलाव
1. ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर होंगे और खुलेंगे 50 मॉड्यूलर अस्पताल
एक तरफ जहां देश के कई शहरों में अस्पताल खोलने पर जोर दिया जा रहा है वहीं पहले से चल रहे अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम तेजी से चल रहा है।अगले पांच सालों में ज्यादातर अस्पताल ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर होंगे। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी से बड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी क्रम में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए अगले दो से 3 महीनों के अंदर देशभर में 50 मॉड्यूलर अस्पताल तैयार करने की योजना बनाई है।
2. आयात होने वाली दवाएं और उपकरण देश में बनेंगे
कोरोना महामारी के दौर में चाहे हाइड्रोक्लोरोक्विन की जरूरत हो या कोरोना वैक्सीन की भारत की फॉर्मा कंपनियों ने पूरी दुनिया को अपनी क्षमता का एहसास कराया है। भारत सरकार ने भी इस क्षेत्र में बड़ा निवेश करने की रणनीति बनाई है। सरकार ने कैंसर व अन्य ऐसी घातक बीमारियों जिनकी दवा अब तक देश में आयात की जाती थी, उनका उत्पादन और रिसर्च करने की रणनीति तैयार की है। अगले पांच सालों में कई ऐसी दवाएं एवं मेडिकल उपकरण जो अब तक आयात होते थे वो अब देश में ही बनाए जाएंगे। इससे जहां मरीजों को सस्ता इलाज मिल सकेगा वहीं इस क्षेत्र में युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिलेगा।
नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय चिकित्सा उपकरणों का बाजार 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जिसके 2025 तक बढ़कर 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है। इसके अलावा भारत का चिकित्सा उपकरणों का निर्यात 2025 तक 10 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।
देश में अब तक जन औषधि स्टोर लगभग 204 प्रकार के सर्जिकल उपकरण मिलते हैं, सरकार का लक्ष्य मार्च 2024 के अंत तक इसे बढ़ा कर 300 सर्जिकल उत्पादों तक विस्तार करना है। जन औषधि केंद्रों पर ज्यादा संख्या में सर्जिकल उत्पाद और दवाएं मिलने से आम लोगों के लिए उचित दाम पर दवा और सर्जिकल उपकरण खरीदना आसान होगा।
3. हेल्थ टूरिज्म पर जोर
हेल्थ टूरिज्म या चिकित्सा पर्यटन भारत में एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है। 2020 के मध्य में, भारत का चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र का अनुमान 5-6 बिलियन अमरीकी डालर का था। अनुमान है कि 2022 तक बढ़कर 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। ऐसे में देश में नए अस्पताल और मेडिकल सेवाओं का विकास होगा।
4. पुराने पेटेंट खत्म होने से खुलेंगे नए अवसरों के दरवाजे
2018 और 2024 के बीच, 251 बिलियन अमरीकी डालर के पेटेंट विश्व स्तर पर समाप्त होने जा रहे हैं। ये भारतीय दवा क्षेत्र के लिए एक बड़ा अवसर है। नीति आयोग के मुताबिक भारत में फार्मास्यूटिकल्स के लिए मौजूदा बाजार का आकार 41 अरब अमेरिकी डॉलर है, जिसके 2030 तक 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
5. टेलीमेडिसिन इंडस्ट्री और होम हेल्थकेयर बढ़ेंगे
भारत में टेलीमेडिसिन इंडस्ट्री 2025 तक बहुत बड़ी हो जाएगी। इसका मार्केट 2025 तक 5410 मिलियन डॉलर तक हो जाने की संभावना है। इस सुविधा के तहत आप घर बैठे एक फोन कॉल के जरिए जरूरी चिकित्सीय परामर्श और दवाएं ले सकेंगे। भारतीय होम हेल्थकेयर मार्केट 2020 में लगभग 6.2 बिलियन अमरीकी डालर था। इसके 2027 तक 21.3 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
आजादी के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र के बड़े पड़ाव
1. देश में इस तरह शुरु हुई आधुनिक चिकित्सा
16वीं शताब्दी से आधुनिक चिकित्सा भारत में आई। आधुनिक चिकित्सा के आने के बाद इस विधा के मेडिकल कॉलेज भी खोलने की आवश्यकता पड़ी। फ्रेंच उपनिवेश के तौर पर पांडिचेरी में 1823 में भारत ही नहीं, बल्कि एशिया का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया। इसके बाद पुर्तगाली उपनिवेश के अंतर्गत गोवा में स्थापित रॉयल हॉस्पिटल को 1842 में मेडिकल कॉलेज में विकसित किया गया। ब्रिटिश शासकों ने 1835 में पहले कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और बाद में मद्रास मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। तीसरा मेडिकल कॉलेज लाहौर में 1860 में खोला गया। किंग जॉर्ज पंचम के 1905 में भारत आने पर भारत के चौथे मेडिकल कॉलेज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया।
आजादी के पहले बने कई एक्ट
1873 में बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट बना
1880 में टीकाकरण अधिनियम तथा 1897 में एपिडेमिक डिजीज एक्ट बनाया गया
1930 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ एक्ट बना
1933 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बना
1939 में पहला रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर एवं ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई
1940 में ड्रग एक्ट की स्थापना भी की गई।
2. 1958 में नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम
आजादी के बाद से अब तक देश में मलेरिया, टीबी, और पोलियो जैसी बीमारियों पर लगाम लगाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया है। और इसमें देश को बड़े पैमाने पर सफलता भी मिली है। आजादी के समय तक देश में हर साल लगभग 10 लाख तक लोगों की मौत मलेरिया से होती थी। इस पर लगाम लगाने के लिए 1958 में नेशनल मलेरिया रेडिकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। किसी एक बीमारी के खिलाफ ये बड़ा हेल्थ प्रोग्राम था। इस अभियान का फायदा मिला और मलेरिया से मरने वालों की संख्या में काफी कमी आई।
3. 1962 से चेचक के खिलाफ बड़ी लड़ाई शुरू
60 के दशक में भी हेल्थ पर काफी काम हुआ। 1961 में देश में पहला एम्स खुला। हालांकि इसका निर्माण 1952 से ही शुरू हो गया था। देश आजाद हुआ उस समय तक चेचक को एक जानलेवा बीमारी माना जाता था। भारत सरकार ने अभियान चला कर अप्रैल 1977 तक इस बीमारी पर काबू पा लिया। ये भी हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि थी।
4. 1977 में रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम
देश में टीबी भी एक बड़ी समस्या था। सरकार ने 1955 में नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया। इसके तहत देश भर में टीबी के विशेष अस्पताल और डिस्पेंसरियां खोली गईं। इस अभियान को और तेज करते हुए अप्रैल 1977 में रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया गया।
5. 1987 में एड्स के खिलाफ मुहिम
एड्स काफी तेजी से फैलने वाली बीमारी है। भारत में ये काफी तेजी से फैल रही थी जिसको देखते हुए 1987 में इसके खिलाफ राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया। इसके लिए सरकार ने 1990-91 तक 29 जोनल ब्लड टेस्टिंग सेंटर बनाए। वहीं देशभर में लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक करने के लिए एक बड़ा अभियान चला। देश में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन बनाया गया।
6. 1995 में शुरू हुआ पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम
भारत सरकार ने देश से पोलियो को खत्म करने के लिए पल्स पोलियो प्रोग्राम की शुरुआत की। देश के लोगों ने भी सरकार के इस अभियान में काफी मदद की और बढ़ चढ़ कर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलवाई। सरकार के इस अभियान का फायदा ये मिला की देश में 2011 के बाद से अब तक पोलियो का कोई नया मामला नहीं पाया गया है।
7. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और शहरी स्वास्थ्य मिशन
2005 में ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) शुरू हुआ। वहीं शहरी स्वास्थ्य मिशन को कैबिनेट के द्वारा 1 मई 2013 को मंजूर किया। इसका लक्ष्य शहरी आबादी के स्वास्थ्य की देखभाल जरूरतों को पूरा करना था। इसका मुख्य फोकस शहरी गरीबों पर था एवं उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य उपलब्ध कराना था। वहीं 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना लांच की गई। इसके जरिए गरीब लोगों को बेहतर और सस्ता इलाज दिलाने का प्रयास किया गया।
आंकड़ों में झलकती कामयाबी
पांच दशक में 28 साल बढ़ गई जीने की उम्र
भारत में पिछले कई दशकों के दौरान जीवन प्रत्याशा में काफी बढ़ोतरी हुई है। 1970-75 के दौरान भारत में जीवन प्रत्याशा जहां करीब 51 वर्ष थी, वहीं 2015-19 में यह बढ़कर 69 वर्ष तक पहुंच गई। औसत जीवन प्रत्याशा दर में वृद्धि भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार निवेश का परिणाम है। विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि शुरुआती दशक (1960-70) में जीवन प्रत्याशा दर 41 से बढ़कर 50 हुई थी, जिसमें उत्तरोत्तर बढ़त जारी है। 1980 से 1990 में जीवन प्रत्याशा दर में 4 साल की बढ़ोतरी हुई। 1980 में जहां यह 54 साल थी, वह 1990 में बढ़कर 58 साल हो गई। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, जीवन प्रत्याशा दर का मतलब है कि कोई भी नौनिहाल तत्कालीन पैटर्न के अनुसार कितने साल तक जीता है।
छह दशकों में घट गई बाल मृत्यु दर, कम हुई 81 फीसदी
किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा आबादी और नौनिहाल बचपन होता है। आजादी के लंबे अर्से तक भारत इस समस्या से जूझता रहा कि घर में बच्चा पैदा होने पर गूंजी किलकारी मातम में बदल जा रही थी। पर बीते कुछ सालों में इसमें काफी कमी आई है। विश्व बैंक द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार अस्पतालों में प्रसव में वृद्धि, नवजात शिशुओं के देखभाल के लिए सुविधाओं का विकास और टीकाकरण बेहतर होने से शिशु मृत्यु दर में कमी आई है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि नवजात शिशुओं की मौत को रोकना और युवा स्वास्थ्य में बढ़ावा देना किसी भी देश के लिए मानव पूंजी का निर्माण एक बुनियादी आधार है जो भविष्य में देश के विकास और समृद्धि में बढ़ावा देगा। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 1960 में प्रति हजार बच्चों में 161 बच्चों की मौत हो जाती थी जबकि 2018 में यह आंकड़ा घटकर 30 रह गया।
- यह भी पढ़े——-
- अफगानिस्तान में परियोजनाओं पर कैसे हुई धन की बर्बादी.
- कैसे हवाई जहाज में उड़ेंगे हवाई चप्पल वाले?
- रक्षाबंधन के दिन आसमान में दिख सकता है ‘ब्लू मून’.
- बक्सर जेल में बीवी के साथ रहता था हत्यारा कैदी, प्रशासन की आंख में धूल झोंककर हुआ फरार